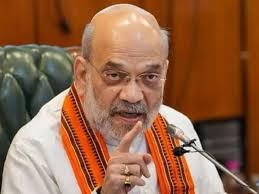बस्तर अब युद्ध-क्षेत्र से विकास-केंद्र की दिशा में कदम बढ़ा रहा है — सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सड़कों, ब्रिज, पर्यटन और जनकल्याण परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, पर साथ ही मानवाधिकार व पर्यावरण संबंधी चिंताएँ भी उठ रही हैं।

1) सुरक्षा और कानून-व्यवस्था
- राज्य सरकार और सुरक्षा बलों ने लक्षित ऑपरेशन्स, पुनर्वास-नीतियाँ और सरेंडर-प्रणालियों पर काम बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्टिंग/आधिकारिक बयानों के अनुसार सैकड़ों नक्सलियों के सरेंडर व कुछ कमजोर किए गए नेटवर्क के बाद प्रशासन यह मानता है कि हालात में सकारात्मक बदलाव आया है।
क्या मायने रखता है: बेहतर सुरक्षा से प्रशासन पहुँच, स्कूल, स्वास्थ्य और बाजार जैसी सार्वजनिक सेवाएँ घाटियों तक पहुँचाने में सक्षम होता है — यही विकास की नींव है।
2) आधारभूत ढांचा और बड़े निवेश
- केंद्र-सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के लिए सड़क-कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (RCPLWEA) के तहत छत्तीसगढ़ को हाल ही में लगभग ₹195 करोड़ आवंटित किए — इससे दूरदराज़ इलाकों में ऑल-वेदर रोड, पुल और क्रॉस-ड्रेनेज का काम होगा। यह कदम विकास को स्थायी पहुँच देने की नीति का हिस्सा है।
- साथ ही राज्य स्तर पर बड़े प्रोजेक्टों की योजना (जल संसाधन/डैम आदि) और औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की तैयारी चल रही है — जिससे रोजगार और स्थानीय आपूर्ति-श्रृंखला विकसित होने की उम्मीद है। (सरकारी घोषणाएँ और बजट दस्तावेज़ों में इन पहलों का जिक्र है।)
3) ब्रिज/रोड व लोक सेवा-पहुँच की तैयारी
- BRO और राज्य एजेंसियों ने बस्तर में कई पुल और सड़क परियोजनाएँ शुरू की हैं; कुछ पुल पूरे हो चुके हैं और बाकी अगले समय में पूरे किए जाने का लक्ष्य बताया गया है — इससे नक्सल प्रभावित इलाकों का बाहरी दुनिया से जुड़ाव तेज होगा।
4) संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन
- बस्तर-दुर्गा/बस्तर-दशहरा जैसी अनूठी परंपराएँ और छत्तीसगढ़ सरकार-लोक प्रयासों के कारण पर्यटन की खपत बढ़ रही है; स्थानीय हस्तशिल्प, पर्व और नेचर-टूरिज्म (Chitrakote, Tirathgarh आदि) से रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। पत्रकार और क्षेत्रीय रिपोर्टों ने “बस्तर मेकओवर” का जिक्र किया है।
5) केंद्रीय/राज्य मान्यता और पब्लिक-डायलग
- राष्ट्रीय स्तर पर भी बस्तर में बदलाव को नोट किया गया है — प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा लिखे गए लेखों/रिपोर्टों को साझा किया, जिससे यह विषय केंद्र सरकार के विमर्श में भी आया।
6) शिक्षा-स्वास्थ्य-समाज: लोककल्याण पहलें
- राज्य में शिक्षा और हेल्थकेयर पहुँचाने के लिए लाइब्रेरी/नालंदा-कम्प्लेक्स जैसे पहलें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता-प्रमाणन जैसी व्यवस्थाएँ भी चल रही हैं — ये लंबे समय में मानवीय पूँजी गढ़ने में मदद करेंगी।
7) पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन
- संस्कृति-सम्बन्धी रीति-रिवाजों (उदा. बस्तर-दुशेरा के लिए बड़े लकड़ी के रथ) के कारण हर साल पेड़ों के कटने की परंपरागत चुनौतियाँ होती रहीं; स्थानीय प्रशासन और समुदाय अब पेड़ लगाने व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपायों पर भी ध्यान दे रहे हैं, पर पर्यावरणविद् जागरूकता और स्थानीय-प्रजाति पुनरोपण पर ज़ोर दे रहे हैं।
8) आलोचना और जोखिम (जो अभी भी बने हुए हैं)
- कुछ मानवाधिकार समूहों और विदेशी मीडिया ने सुरक्षा-ऑपरेशनों के दौरान नागरिकों पर कथित क़दमों (जैसे ‘फेक-एन्काउन्टर’ के आरोप) का हवाला दिया है; इन मुद्दों का समुचित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से निपटना विकास की नैतिक ज़िम्मेदारी है। यह याद रखना जरूरी है कि शांति-प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत मायने रखती है।
निचोड़ (takeaway)
- सुरक्षा-कदमों + इन्फ्रा-निवेश = विकास-दर — बेहतर सड़कों, पुल और सेवाएँ आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था खोल सकती हैं।
- संस्कृति और पर्यटन स्थानीय आजीविका के बड़े स्रोत बन रहे हैं, पर पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन ज़रूरी है।
- चुनौतियाँ भी बाकी — मानवाधिकार, उचित पुनर्वास, जमीन-विवाद और पारदर्शिता पर निरंतर नजर जरूरी है।