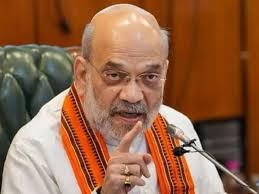छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस और 25 साल की जद्दोजहद..

छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा किस तरह मिला, आयोग कब और कैसे बना, किन-किन व्यवस्थागत कमियों/विवादों से गुजरना पड़ा, और 2025 तक क्या स्थिति बनी — साथ में आगे क्या करने की जरूरत है।
1) संक्षेप — क्या कहलाता है (One-line summary)
छत्तीसगढ़ी को विधायी रूप से राज्य की राजभाषा घोषित किया गया, पर उसके बाद लागू-व्यवहार में कई कमी रह गईं — आयोग बना, पर नामकरण/अध्यक्ष नियुक्ति, शिक्षा में माध्यम बनाना और राजकाज में व्यापक उपयोग जैसी प्राथमिकताओं में लंबे समय तक ठहराव आया।

2) टाइमलाइन — प्रमुख घटनाएँ (दस्तावेजी संदर्भों के साथ)
- 28 नवम्बर 2007 — छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को राज्य की राजभाषा का दर्जा देने वाला विधेयक पारित हुआ (इसी तिथि को बाद में हर साल “छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस” के रूप में मनाया जाता है)।
- 11 जुलाई 2008 / 14 अगस्त 2008 — विधेयक/अधिनियम का प्रकाशन और आयोग का औपचारिक प्रारम्भ; छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग (Chhattisgarhi/Chhattisgarh Official Language Commission) से संबंधित नियम-कानून जारी हुए। आयोग के गठन का प्रावधान और उसके विनियमन प्रकाशित किया गया।
- 2010 — आयोग के गठन/रूल्स पर और स्पष्टता के लिए क़ानूनी ढाँचे (Chhattisgarh Rajbhasha Commission Act) उपलब्ध/लिखित बने। इसमें आयोग की संरचना (अध्यक्ष व सदस्य), कार्यकाल इत्यादि दर्ज है।
- 2010–2024 — आयोग ने कुछ सांस्कृतिक/साहित्यिक कार्यक्रम, प्रकाशित कार्य और ‘माई कोठी’ व ‘बिजहा’ जैसी योजनाएँ प्रारम्भ करने की कहानियाँ रहीं, पर कई योजनाएँ कागजात में अटकी और कार्यान्वयन सीमित रहा। स्थानीय मीडिया-रिपोर्टों में बार-बार यह भी कहा गया कि आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति में देरी ने गतिविधियों को प्रभावित किया।
- 2024–2025 (हालिया) — शिक्षा में मातृभाषा/छत्तीसगढ़ी के उपयोग पर बहस फिर सक्रिय हुई; 2025 के कुछ लोकल रिपोर्टों में प्राथमिक कक्षाओं में छत्तीसगढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल की ख़बरें आईं। (उदाहरण: अगस्त 2025 की रिपोर्ट बताती है कि SCERT छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम पर कार्य कर रहा है)।
3) कानूनी/संस्थागत स्थिति — क्या कानून कहता है और आयोग का स्वरूप
- केंद्र/राज्य के क़ानूनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने Official Language (Amendment) Act, 2007 / 2008 पारित कर राज्य की राजभाषा के दायरे तय किए। (कानूनी दस्तावेज उपलब्ध हैं)।
- बाद में आयोग (Rajbhasha Aayog) का ढाँचा बनाया गया — अध्यक्ष + सदस्य, कार्यकाल, उद्देश्य (भाषा के प्रचार-प्रसार, साहित्यिक कार्य, सरकारी कागजात/आर्थिक व्यवहार में शामिल करने हेतु सुझाव) आदि। पर व्यवहारिक कार्यों के लिए बजट, स्थायी सचिव और नियमित नियुक्तियों का अभाव कई बार रिपोर्ट हुआ।
4) मुख्य समस्याएँ — क्यों ‘न्याय’ नहीं हो पाया (व्यवहारिक कारण)
- आयोग की कार्यशीलता कमजोर रही
स्थानीय मीडिया व प्रतिनिधि रिपोर्टों में बार-बार कहा गया कि आयोग के अध्यक्ष या पूर्ण सदस्य-मंडल की नियुक्तियों में देरी रही — कुछ वर्षों तक अध्यक्ष पद रिक्त रहा, जिससे योजनाएँ रुकीं और प्रकाशन/योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। - नामकरण और प्रतीकात्मक संशोधन के विवाद
कुछ आलोचक कहते हैं कि आयोग का नामकरण-परिवर्तन (यानी ‘छत्तीसगढ़ी’ को अलग से विवक्षित करने के बजाय आधिकारिक नाम में ‘छत्तीसगढ़’ शब्द का प्रयोग) ने भाषा-विशेष की पहचान को कमजोर किया — यह प्रतीकात्मक मुद्दा रहा और अनेक साहित्यकारों/सक्रियों ने इसे भाषा-न्याय में बाधा माना। (स्थानीय साहित्य/नागरिक सक्रियता में यह जिक्र मिलता है)। - राजकाज में वास्तविक समावेशन का अभाव
कागज़ों पर राजभाषा-दर्जा के बावजूद सरकारी कामकाज, नौकरशाही दस्तावेज़, और औपचारिक संचार का प्रमुख माध्यम हिंदी/अंग्रेज़ी रहा — दैनिक राजकीय लेखन और शिक्षा में छत्तीसगढ़ी का उपयोग सीमित रहा। इसलिए ‘माध्यम’ के रूप में अपनाने में देरी/अवरोध दिखा। - शैक्षिक समावेशन में देरी
मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा का सिद्धान्त तो व्यापक रूप से स्वीकार्य है, पर स्थानीय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक-प्रशिक्षण और SCERT-स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के समावेशन में लंबा समय लगा। (हालिया 2025 की खबरें इस दिशा में पहल बता रही - बजट/प्राथमिकता और प्रशासनिक अनुकूलता की कमी
भाषा-संबंधी योजनाओं (पुस्तक प्रकाशन, शब्द-संग्रह, बीजहा/माई-कोठी जैसी योजनाएँ) को धन, 人-शक्ति और प्रशासनिक तवज्जो की आवश्यकता होती है — कई योजनाएँ दस्तावेज़ों तक ही सीमित रहीं।
5) स्थानीय आवाज़ें — नागरिक-साहित्यकार क्या कहते हैं
आपके उदाहरण में जिन व्यक्तियों का उल्लेख है (जैसे डॉ. वैभव बेमेतरि/हार — आपके टेक्स्ट में; और नंदकिशोर सुकुल जैसे साहित्य-सक्रिय) — उनका केंद्रित आरोप यही है कि वैधानिक दर्जा होने के बावजूद व्यवहारिक न्याय नहीं हुआ: न तो शिक्षा-माध्यम बना, न राजकाज में व्यापक उपयोग हुआ, और आयोग का कामकाज ठप पड़ा रहा। स्थानीय संस्थाएँ (छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच इत्यादि) इसी दिशा में लगातार आवाज़ उठाती रही हैं। (यह लोकल-रिपोर्टों और मंचों में देखा गया ट्रेंड है)।
6) हाल की सकारात्मक चालें (2024–2025) — क्या उम्मीद दिख रही है
- शैक्षिक समावेशन के संकेत: अगस्त 2025 की कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम/SCERT मॉड्यूल पर काम चल रहा है — यह अच्छा संकेत है कि मातृभाषा को सीखने की जगह मिल सकती है। पर यह चरणबद्ध और ढीला है — पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए और तैयारी
7) क्या किया जा सकता है — सुझाव (प्रायोगिक और नीति-स्तरीय)
- आयोग का सशक्तीकरण — अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति; स्थायी सचिव और समर्पित बजट; तीन-साल का कार्य-प्लान और पारदर्शी रिपोर्टिंग।
- शिक्षा में चरणबद्ध लागू-करण — पहले प्राथमिक (Class I–V) में मातृभाषा के पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, फिर माध्यम विस्तार; SCERT के मॉड्यूल को तुरंत पायलट जिलों में चलाना।
- राजकाज में प्रयोगात्मक अपनापन — कुछ विभागों/ब्लॉक्स में स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़ी में प्रारम्भिक दस्तावेज़ों, सूचनाओं और जन-सम्पर्क का प्रयोग कर के मॉडल बनाना।
- साहित्यिक संवर्धन व प्रकाशन — ‘माई कोठी’ व ‘बिजहा’ जैसी योजनाओं को वित्तीय संरक्षण और निरन्तरता देना; स्थानीय लेखकों के लिए अनुदान/प्रकाशन-विनिमय।
- जनभागीदारी व जागरूकता — ग्राम-स्तर पर भाषा-वर्कशॉप, शब्द-संग्रह मुहिम, स्कूल/पाठशाला कार्यक्रम — ताकि मातृभाषा का उपयोग जीवन में लौटे।